उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव,2022में कांग्रेस की वर्तमान चुनौतियां और उसके समाधान पर जब भी हम विचार करें-हमें कम से कम उत्तरप्रदेश में पिछले 70 साल के संसदीय लोकतंत्र के इतिहास का सिंहावलोकन करना ही चाहिए। इस दौर के पूर्वार्द्ध में चौधरी चरण सिंह, रामनरेश यादव, बनारसी दास की छोटी-छोटी अवधियों को छोड़ दें, तो कांग्रेस का एकछत्र शासन रहा है, जिस अवधि में गोविंदबल्लभ पंत, डॉ संपूर्णानंद, चंद्रभानु गुप्त, सुचेता कृपलानी, कमलापति त्रिपाठी, हेमवतीनंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, वीपी सिंह, श्रीपति मिश्र, वीरबहादुर सिंह जैसे दिग्गज उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनमें से चौधरी चरण सिंह और वीपी सिंह तो बाद में प्रधानमंत्री भी बने।
पं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, अटलबिहारी बाजपेयी प्रादेशिक राजनीति से प्रोन्नति पाकर राष्ट्रीय राजनीति में नहीं गए, सीधे राष्ट्रीय राजनीति को ही प्रभावित किया, प्रधानमंत्री बने। लेकिन, वह सभी उत्तरप्रदेश की प्रादेशिक राजनीति को अपनी हथेली की रेखाओं की तरह जानते समझते थे। यही कारण है कि भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह मुहावरा अर्थ ग्रहण कर पाया कि दिल्ली की सत्ता की चाभी लखनऊ के रास्ते ही मिल पाती है। इसीलिए, मोदी ने 2014 और 2019 में बनारस को अपना संसदीय क्षेत्र बनाया।
उत्तरप्रदेश में कांग्रेस का वर्चस्व भले 1989 में टूटा हो, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि 1963 में कामराज प्लान में ढूंढ़ी जा सकती है। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के.कामराज ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था कि कांग्रेसियों की सत्ताभिमुखिता जमीनी तौर पर कांग्रेस को अलोकप्रिय बना रही है। अतः,शीर्षपदों पर बैठे कुछ लोगों को सार्वजनिक हित में सत्ता का मोह त्यागकर संगठन कार्य के लिए खुद को समर्पित कर देना चाहिए। कामराज योजना के तहत ही उत्तरप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त को मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा था। लेकिन, कांग्रेस के घटते जनाधारको गतिशीलता मिली थी 1967 में, जब राममनोहर लोहिया ने गैर-कांग्रेसवाद का नेतृत्व किया था।
डॉ राममनोहर लोहिया समाजवाद के शिक्षार्थी रहे थे। वह गंभीरतापूर्वक मानते थे कि सार्वजनिक जीवन में किसी एक व्यक्ति अथवा संगठन का अनवरत वर्चस्व नहीं रहना चाहिए। वह मानते थे कि किसी भी जीवंत,जाग्रत लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि जनसेवक होता है और लोकमत प्रतिकूल होते ही उसे जनप्रतिनिधि के पद से हट जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए। वह कहते थे-लोकतंत्र आंच पर रोटी के समान है,उसे निरंतर उलटते-पलटते रहना चाहिए, तभी वह ठीक से सिंकेगी, वरना जल जाएगी। वह कहते-जिंदा कौमें पांच साल इंतजार नहीं कर सकती। बिहार आन्दोलन या संपूर्ण क्रान्ति आन्दोलन के दौरान जेपी ने इसे ही प्रतिनिधि वापसी के लोकतांत्रिक अधिकार के रूप में चिह्नित किया था और जिसे 2011-12में अण्णा हजारे ने जनांदोलन का मुद्दा बनाया।
डॉ राममनोहर लोहिया पूरी शिद्दत से मानते थे कि समाज के सभी वर्ग राष्ट्र के चतुर्दिक विकास में अपनी सकारात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मक भूमिका निभा सकें, चतुर्दिक विकास का लाभ उठा सकें, इसके लिए जरूरी है कि हर वर्ग में राजनैतिक चेतना विकसित हो, राजनैतिक व्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी हो। वह हरिजन, आदिवासी और पिछड़ों के अपेक्षित विकास के लिए उनमें राजनैतिक जागरण देखना चाहते थे। इसीलिए, उनके दो नारे बहुत लोकप्रिय हुए थे- 1.संसोपा ने बांधी गांठ,पिछड़ा पावै सौ में साठ।
2.जिसकी जितनी भागीदारी,उसकी उतनी हिस्सेदारी।
(संसोपा-संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी-उनकी पार्टी का नाम था।)
1967 में डॉ राममनोहर लोहिया के गैर-कांग्रेसवाद, पिछड़ावाद और सप्त क्रांति ने 1974-77 के दौरान लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रान्ति आन्दोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी, मुंगेरीलाल और बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोगों के गठन का कारण बनी थी।गैर-कांग्रेसवाद के तहत 1977-80 के बीच रामनरेश यादव और बनारसी दास के नेतृत्वमें दो अल्पजीवी सरकारें अस्तित्व में आईं। लेकिन, पिछड़ावाद को मुकाम हासिल हुआ-1989में, जब मुलायम सिंह यादव उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

पंकज श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार “रांची” झारखण्ड

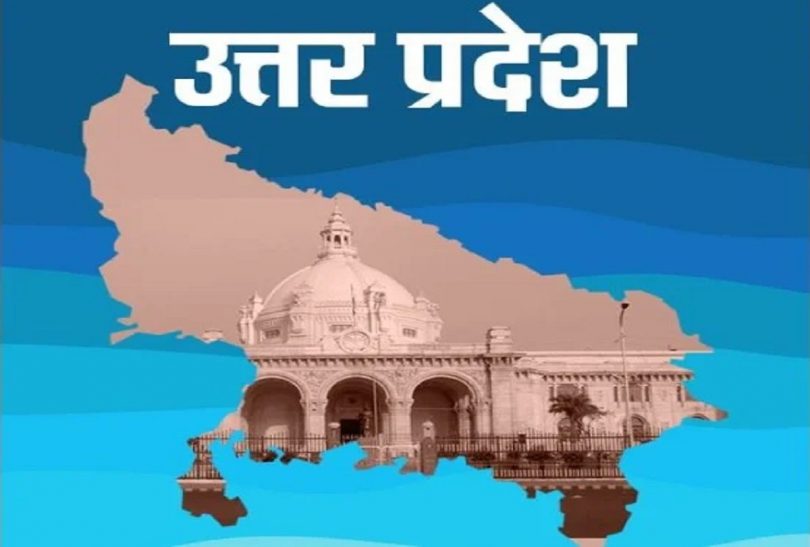






You must be logged in to post a comment.